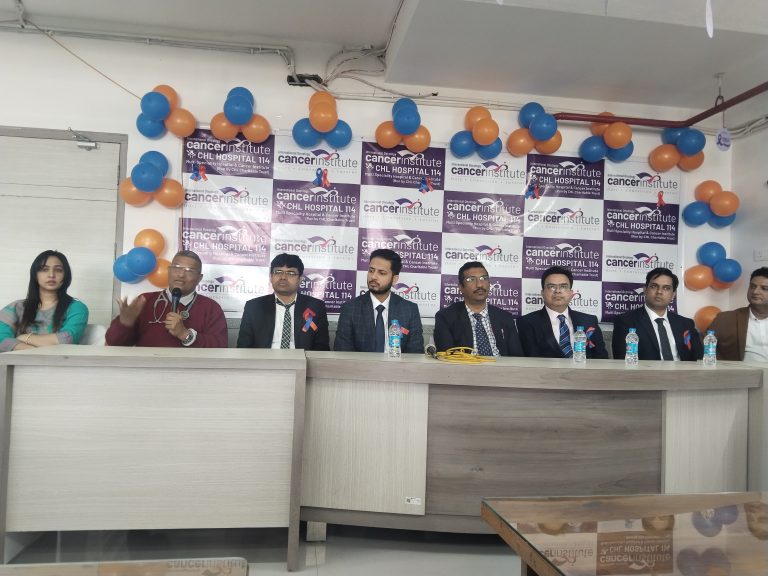डॉ.महेन्द्र यादव की पाती थोड़ी जज़्बाती 
होली का डंडा गड़ने की परंपरा जैसे ही पूरी होती थी, वैसे ही पूरे मोहल्ले में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। युवाओं की टोली जैसे युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हो जाती थी—लकड़ियाँ, कंडे और उपले इकट्ठा करने की होड़ मच जाती थी। हर टोली की चाहत होती थी कि उनकी होली सबसे भव्य और ऊँची हो।
यह वो दौर था जब होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं थी, बल्कि रिश्तों की मिठास, मोहल्ले की आत्मीयता और संगी-साथियों के साथ बिताए गए बेशकीमती पलों का जश्न थी। आधी रात को जैसे ही होलिका दहन होता, मन खिल उठता था। लोगों के चेहरों पर अग्नि की लपटों की रोशनी में एक अलग ही चमक होती थी—भक्ति, उल्लास और साथ रहने की खुशी।
होली की रात: जब रिश्ते गुलाल में घुल जाते थे
जैसे ही होलिका दहन होता, आधी रात से ही रंगों की होली शुरू हो जाती थी। लोग एक-दूसरे को रंगते, हँसी-ठिठोली करते, और हर शिकवे-गिले भुलाकर गले मिलते। यह वो दौर था जब अपनापन सबसे बड़ा रंग था, जो दिलों में उतर जाता था।
रंग पंचमी: जब रंगों की बरसात चरम पर होती थी
होली के कुछ दिन बाद रंग पंचमी आती थी, जो उत्सव का अंतिम पड़ाव होती थी। इस दिन चौराहों पर रंगों से भरे कड़ाव रखे जाते थे, जिसमें आते-जाते लोगों को जबरदस्ती डाल दिया जाता था। न कोई बुरा मानता, न कोई शिकायत करता—यह त्योहार ही ऐसा था, जो हर किसी को एक ही रंग में रंग देता था।
श्री सप्तमी: स्वाद और स्नेह का अंतिम अध्याय
होली का समापन श्री सप्तमी पर होता था, लेकिन यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जब घरों में स्नेह, अपनापन और पारंपरिक स्वाद की महक भर जाती थी। दादी, मम्मी, ताई, काकी सब एक साथ बैठकर गुजिया, बेसन चक्की, बेसन पपड़ी, खस्ता, दही बड़े, पानी पताशी जैसे पारंपरिक पकवान तैयार करती थीं। घर का माहौल खुशबू से भर जाता, और हर कोने से ठहाकों की गूंज सुनाई देती।
श्री सप्तमी केवल पकवान बनाने का नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से जोड़ने का पर्व था। इस दिन पूरे मोहल्ले में एक-दूसरे को घर बुलाने की परंपरा थी। न कोई बुलावे की औपचारिकता, न कोई संकोच—हर कोई हर घर में जाता, प्यार से खिलाता और खिलाया जाता। बड़े-बुजुर्ग खाने की मेज पर बैठकर किस्से-कहानियाँ सुनाते, और बच्चे बेसब्री से पकवानों का इंतजार करते।
अब न वो अपनापन रहा, न वो संगी-साथी
लेकिन अब… अब वह दौर केवल यादों में रह गया है। पहले जो दोस्त बिना बुलाए घर आ जाते थे, अब वे व्हाट्सएप पर शुभकामनाएँ भेजकर औपचारिकता निभा लेते हैं। दादी-नानी के हाथों की बनी गुजिया की जगह अब बाजार की मिठाइयों ने ले ली है। पहले जो रिश्ते त्योहारों पर और गहरे हो जाते थे, अब वे बस सोशल मीडिया तक सिमट गए हैं।
विलासिता की वस्तुएँ हमारे घरों में आ गईं, लेकिन अपनापन पीछे छूट गया। होली का डंडा अब भी गड़ा जाता है, होलिका अब भी जलती है, रंगों की बौछार अब भी होती है, लेकिन वह आत्मीयता, वह उमंग, वह अपनापन… अब नहीं लौटेगा।
वैसी होली अब लौटकर नहीं आएगी…